संघ प्रोटोजोआ (Protozoa)
प्रोटोजोआ संघ के जीव एककोशिकीय (Unicellular) होते हैं तथा इनका पूरा शरीर एक सुकेन्द्रकीय कोशिका के समान होता है। सरलतम् रचना और निम्नतम् कोटि के,“प्रथम जन्तु" हुए भी ये सुगठित बहुकोशिकीय जन्तुओं के समान सभी प्रमुख जैव-क्रियाएँ करते हैं। इसीलिए इन्हें अकोशिकीय (noncellular or acellular) जन्तु भी कहते हैं। इनकी लगभग 64,000 जातियाँ (लगभग 32,000 विद्यमान और 32,000 विलुप्त) ज्ञात हैं। प्रकृति में प्रोटोजोअन जन्तुओं की कुल संख्या किसी भी अन्य संघ के सदस्यों की कुल संख्या से कहीं अधिक है।
संक्षिप्त इतिहास (Brief History)
प्रोटोजोआ का प्रथम अध्ययन लुइवेनहॉक (Leeuwenhoek, 1677) ने अपने सूक्ष्मदर्शी (microscope) की सहायता से किया।
गोल्डफस (Goldfuss, 1817) ने इस संघ को 'प्रोटोजोआ' का नाम दिया। इनके अध्ययन को प्रोटोजोआ विज्ञान (Protozoology) कहते हैं। Smith ने बताया था कि प्रोटोजोआ संघ के सभी जंतु एक कोशिकीय होते हैं।
प्रोटोजोआ के लक्षण (Characters)
प्रोटोजोआ संघ के जंतु विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाते हैं जिनका विवरण इस प्रकार हैं-
1. इस संघ के जंतु जल, गीली मिट्टी, सड़ी-गली कार्बनिक वस्तुओं, आदि में स्वाश्रयी अर्थात स्वतंत्र रूप से(free living) तथा अन्य जन्तुओं एवं पौधों के शरीर में सहजीवी (symbiotic), सहयोजी (commensal) या परजीवी (parasitic) के रूप में रहते हैं। एकाकी या संघीय ।
1. इस संघ के जंतु जल, गीली मिट्टी, सड़ी-गली कार्बनिक वस्तुओं, आदि में स्वाश्रयी अर्थात स्वतंत्र रूप से(free living) तथा अन्य जन्तुओं एवं पौधों के शरीर में सहजीवी (symbiotic), सहयोजी (commensal) या परजीवी (parasitic) के रूप में रहते हैं। एकाकी या संघीय ।
2. इस संघ के जंतुओं का शरीर अतिसूक्ष्म लगभग(0.001 - 3.00 मिमी) तक होता है जिसे हम खुली आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। इन्हें प्रायः सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता हैं।
3. इनके शरीर की आकृति विविध प्रकार की होती है। जो प्रायः जाति के अनुसार स्थाई, कुछ वातावरणीय दशाओं में तथा कुछ आयु या गमन की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील होते रहते हैं।
4. इनका शरीर नग्न या महीन झिल्ली द्वारा ढका रहता है जिसे पेलिकल कहते हैं। जबकि कुछ जंतुओं में उनका शरीर कठोर खोल में बन्द रहता है।
5. इनके एककोशिकीय शरीर में जटिल यौगिकों के अणुओं से बनी तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विविध प्रकार की विशिष्ट रचनाएँ होती है जिन्हें अंग (organs) न कहकर अंगक (organelles) कहते हैं। ये अन्तःकोशिकीय (intracellular) “श्रम विभाजन (division of labour)” प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए प्रोटोजोआ को “जीवद्रव्य के स्तर पर गठित (protoplasmic level of body organization) जन्तु" कहते हैं।
6. ऐसे संघ के जंतुओं में गमन के लिए पादाभ (pseudopodia), कशाभिकाएँ (flagella), या रोमाभ (cilia) होते हैं जिसके द्वारा यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं।
7. इन जंतुओं में एक, दो या कई समान केन्द्रक (nuclei) होते हैं जबकि कुछ में केन्द्रक दो प्रकार के भी होते हैं।
8. इन जंतुओं में पोषण की विधियां क्रमशः प्राणिसम (holozoic), पादपसम (holophytic) व मृतोपजीवी (saprophytic or saprozoic) होती है तथा कुछ जंतु परजीवी (parasitic) भी होते हैं। कई जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक पोषण विधियाँ (मिश्रपोषी-mixotrophic) होती है। प्राणिसम सदस्यों में पाचन खाद्य-धानियों (food-vacuoles) में होता है।
9. इनमें गैसीय विनिमय तथा उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। यह शरीर की सतह से सामान्य विसरण (diffusion) द्वारा पूरी होती है।
10. आवश्यकता पड़ने पर शरीर में जल की मात्रा के नियन्त्रण (परासरण नियन्त्रण osmoregulation) के लिए एक या अधिक संकुचनशील रिक्तिकाएँ (contractile vacuoles) बनने लगती हैं। जिसके द्वारा यह अपने शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं।
11. वातावरणीय परिवर्तनों, अर्थात् उद्दीपनों (stimuli) के अनुसार इनकी प्रतिक्रियाशीलता (responsivity) अत्यधिक सरल होती है।
12. इनमें जनन, अलैंगिक (asexual) अथवा लैंगिक (sexual) दोनों विधियों द्वारा होता है। जनन के लिए या प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में सुरक्षा के लिए, परिकोष्ठन (encystment) की व्यापक क्षमता का विकास होता है।
प्रोटोजोआ संघ में इनके गमनांगकों (Travelers) एवं केंद्रकों के आधार पर, इसे चार उप संघों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
उपसंघ सार्कोमैस्टिगोफोरा (Subphylum Sarcomastigophora)
- उपसंघ सार्कोमैस्टिगोफोरा (Subphylum Sarcomastigophora)
- उपसंघ स्पोरोजोआ (Subphylum Sporozoa)
- उपसंघ निडोस्पोरा (Subphylum Cnidospora)
- उपसंघ सिलियोफोरा (Subphylum Ciliophora)
इस उपसंघ के जंतुओं में गति करने के लिए गमनांगक पादाभ (Moving feet), या कशाभिकाएँ (flagellates), या दोनों ही पाये जाते हैं। इनमें केन्द्रक एक या अधिक हो सकते हैं लेकिन एक से अधिक होने पर भी सब समान रहते हैं।
इन्हें तीन वर्गों में बाँटा गया है-
इन्हें तीन वर्गों में बाँटा गया है-
1. वर्ग मैस्टिगोफोरा या फ्लैजेलैटा (Class Mastigophora or Flagellata) : इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं-
(i) गमनांगक एक या अधिक महीन धागे सदृश कशाभिकाएँ (flagella)
(ii) अनेक सदस्य पादपों की भाँति पर्णहरिमयुक्त अर्थात् क्लोरोफिलयुक्त। उदाहरण- यूग्लीना (Euglena)। परजीवी ट्रिपैनोसोमा (Trypanosoma) जिसके संक्रमण से अफ्रीकी निद्रारोग (sleeping sickness) हो जाता है। इसे ग्लोसाइना पाल्पैलिस (Glossina palpalis) नामक जाति का कीट फैलाता है।
Read more - यूग्लीना क्या है?(EUGLENA)
(i) गमनांगक पादाभ पाए जाते हैं।
(ii) शरीर की आकृति प्रायः परिवर्तनशील रहती है। उदाहरण- अमीबा (Amoeba), परजीवी एन्टअमीबा (Entamoeba)।
Read more - अमीबा (AMOEBA)
3. वर्ग ओपैलाइनैटा (Class Opalinata) : इस वर्ग के जंतुओं के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं-
(i) इस वर्ग के सभी जंतु चपटे होते हैं जो ऐम्फीबिया वर्ग के जीवो की आँत के परजीवी के रूप में पाए जाते हैं।
(ii) कोशिकामुख (cytostome) अनुपस्थित रहते हैं।
(iii) गमनांगक अनेक रोमाभसदृश छोटी-छोटी कशाभिकाओं द्वारा होता है।
(iv) केन्द्रक दो या अधिक, सब समान।
(v) जनन संयुग्मन (conjugation) द्वारा नहीं होता है। उदाहरण- ओपैलाइना (Opalina)।
उपसंघ स्पोरोजोआ (Subphylum Sporozoa)
इस संघ के जंतु अन्य जन्तुओं या पादपों के अन्तः परजीवी (endoparasites) के रूप में रहते हैं। अतः इनमें विशिष्ट गमनांगक एवं संकुचनशील रिक्तिकाएँ अनु पस्थित रहती हैं। इनका जीवन-वृत्त प्रायः जटिल होता है। इसमें यह बीजाणुजनन (sporogenesis) द्वारा होता है। इन बीजाणुओं में ध्रुवीय तन्तु (polari filaments) नहीं होते हैं।
स्पोरोजोआ को बीजाणुओं की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बाँटा गया हैं-
1. वर्ग टीलोस्पोरिया (Class Telosporea) : बीजाणुक (sporo zoites) लम्बवत् और प्रायः बीजा णुओं में । उदाहरण–प्लाज्मोडियम (Plasmodium); मोनोसिस्टिस (Monocystis)।
2. वर्ग पाइरोप्लाज्मिया (Class Piroplasmea): पशुओं के लाल रुधिराणुओं के अतिसूक्ष्म परजीवी जिनमें बीजाणु नहीं बनते, अर्थात् बीजाणुक नग्न होते हैं। इनसे पशुओं में टेक्सास ज्वर (Texas cattle fever) नामक रोग होता है। उदाहरण बैबेसिया (Babesia)।
Read more - परासरण नियन्त्रण (Osmoregulation) क्या है?
उपसंघ निडोस्पोरा (Subphylum Cnidospora)
स्पोरोजोआ की भाँति यह अन्य जन्तुओं के शरीर में परजीवी की तरह रहते हैं। इनमें गमनांगकों एवं संकुचनशील रिक्तिकाओं का अभाव रहता है तथा इनके जीवन वृत्त में बीजाणुजनन होता है और बीजाणु बनते हैं, परन्तु, स्पोरोजोआ के विपरीत, इनके बीजाणुओं में ध्रुवीय तन्तु होते हैं।
निडोस्पोरा को भी, बीजाणुओं के विकास की विधि के आधार पर, दो वर्गों में बाँटा गया है
1. वर्ग मिक्सोस्पोरिया (Class Mixosporea) : इस वर्ग के जंतुओं के बीजाणुओं का विकास कई केन्द्रकों से होता है। इनके बीजाणु-खोल दो या तीन कपाटों (valves) के बने होते हैं। उदाहरण-सीरैटोमिक्सा (Ceratomyxa) ।
2. वर्ग माइक्रोस्पोरिया (Class Microsporea) : (i) इस बार के जंतुओं के बीजाणुओं का विकास एक केन्द्रक से होता है तथा इनके बीजाणु खोल एक ही कपाट का बना होता है। उदाहरण-नोसीमा (Nosema)।
उपसंघ सिलियोफोरा (Subphylum Ciliophora)
एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए इनके पास रोमाभ (cilia) उपस्थित रहते हैं । कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें इनके स्थान पर वयस्क में भोजन ग्रहण के लिए प्रचषक स्पर्शक (sucking tentacles) उपस्थित रहते हैं। इनमें केंद्रक दो या अधिक होते हैं तथा दोनों दो प्रकार के होते हैं एक बड़ा गुरुकेन्द्रक (macronucleus) और एक या अधिक छोटे लघुकेन्द्रक (micronuclei)। इनमें जनन संयुग्मन (conjugation) द्वारा भी होता है।
FAQs
1. प्रोटोज़ोआ से कैसे छुटकारा पाएं?
प्रोटोज़ोआ से छुटकारा पाने के लिए, आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किस प्रकार के प्रोटोज़ोआ से संक्रमित हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप किस प्रकार के प्रोटोज़ोआ से संक्रमित हैं, तो आप एक एंटीप्रोटोज़ोअल दवा ले सकते हैं। एंटीप्रोटोज़ोअल दवाएं प्रोटोज़ोआ को मारने या उनके विकास को रोकने के लिए काम करती हैं।
2. प्रोटोज़ोआ मनुष्यों को कैसे संक्रमित करते हैं?
प्रोटोज़ोआ मनुष्यों को कई तरह से संक्रमित कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- भोजन या पानी के माध्यम से: प्रोटोज़ोआ दूषित भोजन या पानी के माध्यम से मनुष्यों में प्रवेश कर सकते हैं।
- मच्छरों या अन्य कीड़ों के माध्यम से: कुछ प्रोटोज़ोआ मच्छरों या अन्य कीड़ों द्वारा मनुष्यों में फैलते हैं।
- सीधे संपर्क के माध्यम से: कुछ प्रोटोज़ोआ सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं।
3. प्रोटोज़ोआ का उदाहरण क्या है?
प्रोटोज़ोआ के कई उदाहरण हैं, जिनमें शामिल हैं:
- प्लास्मोडियम: इस प्रोटोज़ोआ से मलेरिया होता है।
- ट्रिपैनोसोमा: यह प्रोटोज़ोआ sleeping sickness का कारण बनता है।
- लैम्ब्लिया: इस प्रोटोज़ोआ से आंतों के संक्रमण होता है।
- एचिसटोप्लाज़्मा: इस प्रोटोज़ोआ से फेफड़ों का संक्रमण होता है।
- जिआर्डिया: यह प्रोटोज़ोआ भी आंतों के संक्रमण फैलाता है।
4. प्रोटोज़ोआ के कारण होने वाले तीन मानव रोग कौन से हैं?
प्रोटोज़ोआ के कारण होने वाले तीन सबसे आम मानव रोग हैं:
- मलेरिया: मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। मलेरिया के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं।
- सोने की बीमारी (Sleeping sickness): Sleeping sickness एक गंभीर बीमारी है जो ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोज़ोआ के कारण होती है। Sleeping sickness के लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान।
- आंतों के संक्रमण: प्रोटोज़ोआ आंतों के संक्रमण का कारण बन सकते हैं, जो दस्त, पेट दर्द और पेट फूलने का कारण बन सकते हैं।
5. प्रोटोज़ोआ का संचारण कैसे होता है?
प्रोटोज़ोआ के संचरण के तरीके इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा प्रोटोज़ोआ शामिल है। कुछ प्रोटोज़ोआ दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलते हैं, जबकि अन्य संक्रमित कीड़ों के काटने के माध्यम से फैलते हैं। यौन संपर्क के माध्यम से भी कुछ प्रोटोज़ोआ फैल सकते हैं।
.jpg)

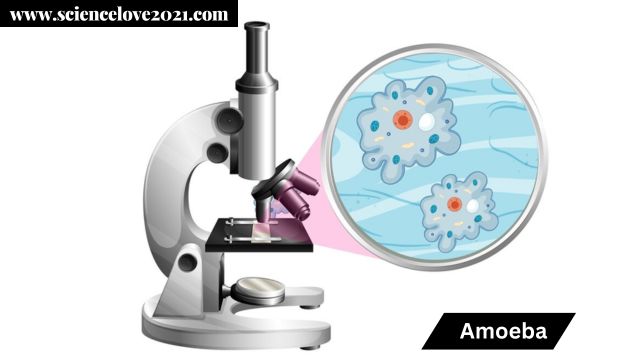
.jpg)


No comments:
Post a Comment